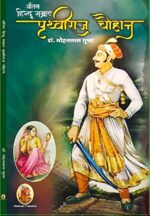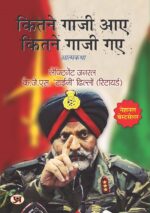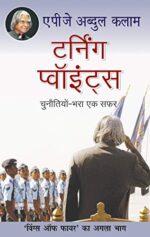जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download Free in this Post from Google Drive Link and Telegram Link ,
All PDF Books Download Free and Read Online, जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download PDF , जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download Summary & Review. You can also Download such more Books Free - Hindi Autobiography PDF DownloadHindi PDF Books DownloadDescription of जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download
| Name : | जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download |
| Author : | |
| Size : | 1.9 MB |
| Pages : | 129 |
| Category : | Biography / Autobiography |
| Language : | Hindi |
| Download Link: | Working |
Jalti Hui Nadi Book PDF Download प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर की आत्मकथा के दो खंड प्रकाशित होकर बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं। ये एक व्यक्ति से जुड़े होने पर भी अपने-आप में स्वतंत्र हैं और समय के क्रम में मोटे तौर पर ही चलते हैं। तीसरे खंड, ‘जलती हुई नदी’ की थीम भी एक रहस्यमयी स्त्री से बँधी आरम्भ से अंत तक चलती है। उसी के साथ वे व्यक्तियों और घटनाओं को अपनी विशिष्ट ईमानदारी और बेबाकी के साथ साहित्य, कला और फिल्म की कहानी कहते चलते हैं। बंबई के फिल्म-जगत में प्रतिष्ठित होने वाले कमलेश्वर हिन्दी साहित्य के पहले अग्रणी लेखक थे, और इस दुनिया का चित्रण भी उनका सबसे अलग और विशिष्ट है। ये झांकियाँ बहुत आकर्षक बन पड़ी हैं।
Summary of book जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download
ख़तवाली, रूमाल और कर्ज़े की रसीदें!
तो, अब आगे का सिलसिला। वहीं से यह शुरुआत, जहाँ एक नितान्त रहस्यमयी सृष्टि अपनी तलाश के लिए लेखक को पुकार रही थी!
एक ख़त, दो ख़त, तीसरा ख़त और फिर कई ख़त!
वैसे तो वो इस तरह के ख़तों का आदी था लेकिन इन ख़तों में समाई कशिश और पुकार कुछ दूसरी ही थी। लिखावट भी कुछ ऐसी कि जैसे मन कुछ कहता गया हो और हाथ सिर्फ़ लिखता गया हो। “तुम हर हफ़्ते मेरे कमरे में आ बैठते हो…” में तुम का “तु” उसके “म” पर दाँत की तरह चढ़ गया था… “मैं उस समय ब्लाउज़ बदल रही थी…और तुम कुछ बोलते हुए मुझे देख रहे थे…”
…“अब तो यह आदत-सी पड़ गई है…कमरे में तुम्हारे आने से पहले मैं ख़ूब जी भर कर नहाती हूँ। बाथरूम की लाइट चाँदनी की तरह मेरे जिस्म पर पड़ती है…मैं चाँदनी में नहा-नहा जाती हूँ…बिजलियाँ-सी बदन में लहकती और टूटती हैं…तब तक तुम्हारे आने की आहट होती है…तुम्हारे आने से पहले साज़ बजते हैं …बम्बई की सड़कें दुबली हो जाती हैं, बिल्डिंगों के कम्पाउण्ड ख़ाली हो जाते हैं और लोग तुमसे मिलने अपने घरों में लौट आते हैं…मैं बाथरूम से निकल कर सीधी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हूँ…आज परफ़्यूम मैंने तुम पर भी स्प्रे कर दिया था, महक तुम तक पहुँची?”…वही–ख़तवाली।
ख़तवाली! ख़त तो आते थे लेकिन पता लेकर नहीं आते थे। सैकड़ों ख़तों में से सेक्रेटरी कुछ ख़त बिना खोले रख देता था–जो उसे पर्सनल-से लगते थे। उन्हीं में दूसरा और तीसरा ख़त खोल लेने के बाद वह ऐसे ख़तों को पहचानने लगा था और अब उन्हें बिना खोले ही रख देता था। ख़तों की तादाद में वे ख़त या इस तरह के ख़त कुछ अलग से ही लगते-दिखते थे…सर्दियों में आनेवाले दूर-दराज़ के पंछियों की तरह।
ख़तवाली के ख़तों का सिलसिला फ़ोन आने के बाद टूटा–हलो! पहचाना मुझे?
आवाज़ में ख़तों से ज़्यादा कोहरा और कशिश थी। जैसे कोई धुंधली आवाज़ सुबह के नम कोहरे के पार से बोल रही हो।
उस पर कुछ बीता। मगर इतना नहीं कि वजूद की चट्टानें हिल जाएँ या तड़क जाएँ…
ख़तवाली ने ख़ामोशी को तोड़ा–हलो! कुछ बात तो कीजिए!
–किस सिलसिले में!
–सिलसिले तो आगे बनेंगे…
–आप कुछ अपने बारे में बताएँगी!
–क्यों, क्या अब भी नहीं पहचाना? मैं हूँ ख़तवाली!
–ओह, आप!
–मिलेंगे कभी।
–जब आप कहें।
–कहाँ? किस जगह…अभी आ जाइए न…
–अभी…अभी तो मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ।
–तो इधर से होते हुए निकल जाइए।
–आप कहीं पास से बोल रही हैं?
–हां, आपके घर से कुछ दूर…
–मेरा घर आपको मालूम है?
–आपके बारे में मुझे क़रीब-क़रीब सब कुछ मालूम है। आपकी एक ख़ूबसूरत-सी बच्ची है, उसे छोड़ने आप नीचे तक आते हैं, मैंने कई बार देखा है क्योंकि मैं आपके घर के सामने से रोज़ गुज़रती हूँ…दूर से आपको कई बार देखा है, अब नज़दीक से देखना चाहती हूं, बिलकुल नज़दीक से। इधर से होते हुए निकल जाइए न!
–किधर से?
–पैडर रोड से। मैं वैलवर्थ पर खड़ी मिलूँगी…बाहर…
–वैलवर्थ तो राइट पर पड़ेगा…
–मैं आपको ज़हमत नहीं दूंगी…मैं क्रास करके चली आऊँगी!
–लेकिन मैं आपको पहचानूंगा कैसे?
–मैं तो पहचानती हूँ आपको। मैं खुद ही चली आऊँगी। ट्रेफ़िक के बावजूद जो सड़क पार करके आपकी तरफ़ आता दिखाई दे, समझ लीजिएगा, वही मैं हूँ!
–जी!…कहते हुए वह थोड़ा-सा अटका था।
–मुझे देखकर आपको पछतावा नहीं होगा! तो, दस मिनट बाद…आधे घंटे या दो घंटे बाद…या फिर महीनों-बरसों बाद! मैं ता-उम्र आपको वहीं खड़ी मिलूंगी! आप वक़्त, दिन, महीना और बरस बता दीजिए…
वह जैसे किसी बारिश में एकाएक अंदर तक भीग गया था। बम्बई की इस दुनिया में उसने चलती और भागती हुई तो बहुत-सी सड़कें देखी थीं, पर ऐसी रुकी हुई सड़क नहीं देखी थी।
उसे लगा जैसे यह ख़तवाली पुरानी किताबों के पन्नों से निकल कर आई है–कोई पार्वती, कोई चंद्रमुखी, कोई सुधा…
आहत, अवसन्न और ख़ामोश अतीत कब कैसे एकाएक अपना मरुथल लाँघ कर कहीं दूर से पुकारने लगता है…इसका बहुत तेज़ एहसास उसे हुआ था।
वह एक बंजर ज़मीन से आया था। ख़ामोश आकर्षणों की दुनिया से, जहाँ कहा कुछ भी नहीं जाता। मन-ही-मन में कुछ अरमान करवटें लेते हैं, अनबूझी इच्छाएँ आती और चली जाती हैं…और क़स्बाई सपने ख़तों पर फैले कपड़ों की तरह धूप उतरते ही बटोर लिए जाते हैं…कुछ अनकहे धुँधले-से अक्स स्मृतियों में उलझे रह जाते हैं–जो न घटते हैं, न बढ़ते हैं…बस, पानी के दाग़ की तरह वजूद के लिबास पर नक्श हो जाते हैं, जिन्हें सिर्फ़ आप ही देख सकते हैं।
उसका पूरा क़स्बा, क़स्बे के मोहल्ले की कई खिड़कियाँ तब उसे मौन हसरत से देखती नज़र आई थीं, जिन्होंने कहना तो बहुत कुछ चाहा था, पर कभी कुछ कहा नहीं था। किसी खिड़की में कोई काजल लगी आँख उलझी थी, किसी में इशारा करती कोई उँगली, किसी में शरमा कर लौटते हुए अधूरे अरमान और किसी में मजबूरी की कोई दास्तान…
ऐसी ही एक दास्तान उसे बार-बार याद आती है। तब वह बी. एस-सी. फ़र्स्ट ईयर छोड़कर कला-फ़ैकल्टी में आ गया था। क्यों आ गया था, यह खुद उसे पता नहीं था। उन दिनों भविष्य कहीं था ही नहीं…एक व्यर्थ वर्तमान साथ था, जो बस–चलता जाता था। यह आज़ादी से तत्काल पहले का दौर था। उन दिनों रेलगाड़ियों में रिज़र्वेशन की सुविधा और सिस्टम नहीं था। अब उसे याद नहीं–विद्या किस फ़ैकल्टी में थी, पर छुट्टियाँ साथ-साथ होती थीं, इसलिए वे दोनों इलाहाबाद स्टेशन पर मिल ही जाते थे। विद्या फ़तेहगढ़ की थी–जहाँ की उसकी पत्नी गायत्री हैं, पर तब गायत्री का पता कहाँ था। तो छुट्टियों में अपने-अपने घर जाने के लिए एकाध बार तो विद्या से ऐसे ही उसकी मुलाक़ात हुई, पर फिर वे दोनों इलाहाबाद स्टेशन पर एक-दूसरे का इन्तज़ार करने लगे। न मालूम यह कैसा लगाव था कि प्लेटफ़ार्म पर वे तब तक रुके रहते थे, जब तक दूसरा आ नहीं जाता था। अनकहे तरीक़े से यह तय हो गया था कि छुट्टी होने वाले दिन की सुबह पहली पैसिंजर गाड़ी से ही सफ़र किया जाएगा। उन दिनों भी कुछ तेज़ एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती थीं, पर उन्हें पैसिंजर ही पसन्द थी, जो धीरे-धीरे चलती, हर स्टेशन पर रुकती जाती थी।
उन्हें छोटे-छोटे स्टेशनों के नाम भी पहाड़े की कड़ी की तरह याद हो गए थे। अब बमरौली आएगा, अब मनौरी, अब सैयद सरावां और फिर भरदारी, सिराथू, फ़तेहपुर और फिर…फिर कानपुर। स्टेशनों के नाम वे दोनों साथ-साथ पढ़ते थे और किस स्टेशन पर कितनी जल-क्षमता वाली टंकी लगी है यह भी उन्हें याद था। इंजन किस स्टेशन पर पानी लेगा, यह भी पता था। चाहते तो दोनों ही नहीं थे, लेकिन कानपुर स्टेशन आ ही जाता था।
विद्या यहीं उतर कर फ़तेहगढ़ जाने वाली गाड़ी बदलती थी। कानपुर से उसे छोटी लाइन पकड़नी होती थी, जिसका प्लेटफ़ार्म काफी दूर था। उन दिनों टाटा या बॉय-बॉय नहीं होता था। विद्या चुपचाप उतरती थी। वह उसका झोला या किताबों का बस्ता उठाकर थमा देने में मदद कर देता था और वह “अच्छा” कहकर पुल पर चढ़कर उस पार वाले प्लेटफ़ार्म पर अपनी गाड़ी पकड़ने चली जाती थी। वह उसे छोड़ने या विदा देने नहीं जा पाता था, क्योंकि तब तक उसकी गाड़ी छूट सकती थी।
उसका सफ़र शिकोहाबाद तक जारी रहता था, जहाँ से वह ब्रांचलाइन की गाड़ी पकड़ कर मैनपुरी पहुँचता था। बीच में सिर्फ़ तीन स्टेशन पड़ते थे।
कोसमा स्टेशन उसे आज भी याद है क्योंकि यह ऐसा स्टेशन था, जिसे वह कभी भूल ही नहीं सकता था! कोसमा गाँव में अमर शहीद बिस्मिल की छोटी बहन शास्त्री देवी उन दिनों रहती थीं, जो क्रांतिकारियों के हथियार अपने लहँगे में छुपाकर मीलों-मील पहुँचाया करती थीं। पैदल।
आज़ादी के बाद इन “जिज्जी” की दुर्दशा हो गई थी। जिन दिनों वह दिल्ली में था तो उसने जिज्जी के लिए कुछ चंदा भी जमा किया था। चंदे की मामूली-सी रक़म लेकर वह दो दोस्तों के साथ जिज्जी को देने गया था। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वे लकवे या गठिया से बुरी तरह ग्रस्त थीं। आँखों से दिखाई भी कम पड़ता था। जीभ भी लड़खड़ाने लगी थी।
कोसमा जानेवाला वह दिन उसे अच्छी तरह याद है। प्लेटफ़ार्म एकदम नीचा है। डिब्बे का हैंडिल थाम कर वह तीनों पायदान उतरा था। आज़ादी के उन दिनों तक, रेलगाड़ी से बिना टिकट सफ़र करने वालों का बोलबाला हो चुका था। स्टेशन पर एक ख़लासी और एक ही बाबू होता था। वही बाबू लोहे के छोटे-से गेट पर टिकट जमा करता था। बिना टिकट वाले मुसाफ़िर डिब्बों से कूद कर खेतों की तरफ़ ताबड़तोड़ भागते थे। ज़्यादातर वे उल्टी तरफ़ उतरकर भागते थे, ताकि दिखाई ही न पड़ें। जो साहस करके सीधी तरफ उतरकर भागते थे, उन्हें पकड़ने के लिए काफी दूर तक टिकट बाबू और ख़लासी पीछा करते थे। पर गाड़ी को जाना होता था और जब तक ख़लासी लबिया न बजा दे, तब तक गाड़ी छूट नहीं सकती थी। गार्ड साहब हुर्रे वाली सीटी बजाते और हरी झंडी फहराते थे, तब रहकने वाली सीटी बजाकर इंजन भाप के बादल छोड़ता और गाड़ी धक-धक करती चली जाती थी। इंजन का उगला हुआ काला धुआँ देर तक ठहरा रहता था, फिर हवा से छितरा जाता था। रेलगाड़ी की धमक पगडंडियों में समाई रहती थी।
ऐसी ही एक पगडंडी से होता हुआ वह जिज्जी के गाँव पहुँचा था। सरसों में दाने पड़ गए थे। अरहर में अभी पीले फूल बाकी थे। गेहूँ और जौ पकने के लिए तैयार खड़े थे। आज़ाद भारत की फ़सलें तो लहरा रही थीं, पर जिज्जी का चूल्हा बुझा और पतीली ख़ाली पड़ी थी। पास के घर से कुछ खाना आ जाता था।
उन्हें उसने बड़े संकोच से चंदे की थोड़ी-सी रकम देने की बात कही थी और रुपए सामने रखे थे तो बड़ी मुश्किल से जिज्जी ने लटपटाती ज़ुबान से कुछ कहा था, और कुछ रुककर कथरी के उस पार आले में रखे सामान की ओर इशारा किया था। आले में तम्बाकू की एक पुड़िया थी, कालिख से भरी एक ढिबरी, शायद जुशांदे की पुड़िया और मटमैली-सी एक कितबिया थी–मुड़ी-तुड़ी पापड़ की तरह। तब जिज्जी ने बहुत मुश्किल से जो कुछ कहा था, वह लगभग यही था–
जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download link is given below
We have given below the link of Google Drive to download in जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download Free, from where you can easily save PDF in your mobile and computer. You will not have to pay any charge to download it. This book is in good quality PDF so that you won't have any problems reading it. Hope you'll like our effort and you'll definitely share the जलती हुई नदी / Jalti Hui Nadi Book PDF Download with your family and friends. Also, do comment and tell how did you like this book?
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]