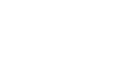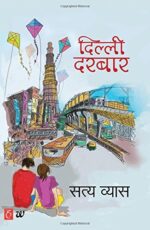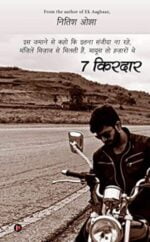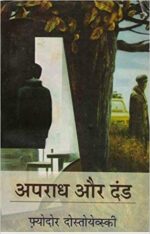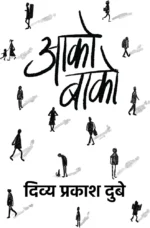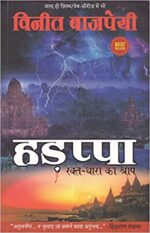श्रीकृष्ण अर्थात हजारो वर्षो से व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से भारतीय जनमानस में व्याप्त एक कालजयी चरित्र एक युगपुरुष! श्री कृष्ण चरित्र के अधिकृत संदर्भ मुख्यतः श्रीमद भागवत, महाभारत हरिवंश और कुछ पुराणों में मिलते है इन सब ग्रंथों में पिछले हजारों वर्षों से श्री कृष्ण चरित्र पर सापेक्ष विचारों की मनघढन्त परतें चढ़ती रहीं यह सब अज्ञानवश तथा उन्हें एक चमत्कारी व्यक्तित्व बनाने के कारण हुआ फलत आज श्रीकृष्ण वास्तविकता से सैंकड़ो योजन दूर जा बैठे हैं. श्री कृष्ण शब्द ही भारतीय जीवन प्रणाली का अनन्य उद्गार है, आकाश में तपता सूर्य जिस प्रकार कभी पुराना नहीं हो सकता उसी प्रकार महाभारत कथा का मेरुदंड– यह तत्वज्ञ वीर भी कभी भारतीय मानस पटल से विस्मृत नहीं किया जा सकता. जन्मतः ही दुर्लभ रंग्सुत्र प्राप्त होने के कारण कृष्ण के जीवन चरित्र में भारत को नित्यनुतन और उन्मेषशाली बनाने की भरपूर क्षमता है. श्री कृष्ण जीवन के मूल संधर्भो की तोड़-मरोड़ किये बिना क्या उनके युगंधर रूप को देखा जा सकता है क्या उनके सवच्छ नीलवर्ण जीवन सरोवर का दर्शन किया जा सकता है क्या गीता में उन्होंने भिन्न-भिन्न योगो का मात्र निरूपण किया है सच तो यह है कि श्रीकृष्ण की जीवन सर्वोअर पर छाए शैवाल को तार्किक सजगता से हटाने पर ही उनके युगन्धररूप के दर्शन हो सकते है.
Summary of book युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download
युगन्धर
श्रीकृष्ण—अर्थात् हजारों वर्षों से व्यक्त एवं अव्यक्त रूप से भारतीय जनमानस में व्याप्त एक कालजयी चरित्र—एक युगपुरुष!
श्रीकृष्ण-चरित्र के अधिकृत सन्दर्भ मुख्यत: श्रीमद्- भागवत, महाभारत, हरिवंश और कुछ पुराणों में मिलते हैं। इन सब ग्रन्थों में पिछले हजारों वर्षों से श्रीकृष्ण-चरित्र पर सापेक्ष विचारों की मनगढ़न्त परतें चढ़ती रहीं। यह सब अज्ञानवश तथा उन्हें एक चमत्कारी व्यक्तित्व बनाने के कारण हुआ। फलत: आज श्रीकृष्ण वास्तविकता से सैकड़ों योजन दूर जा बैठे हैं।
‘श्रीकृष्ण’ शब्द ही भारतीय जीवन-प्रणाली का अनन्य उद्गार है। आकाश में तपता सूर्य जिस प्रकार कभी पुराना नहीं हो सकता, उसी प्रकार महाभारत कथा का मेरुदण्ड—यह तत्त्वज्ञ वीर भी कभी भारतीय मानस-पटल से विस्मृत नहीं किया जा सकता। जन्मत: ही दुर्लभ रंगसूत्र प्राप्त होने के कारण कृष्ण के जीवन-चरित्र में, भारत को नित्यनूतन और उन्मेषशाली बनाने की भरपूर क्षमता है।
श्रीकृष्ण-जीवन के मूल सन्दर्भों की तोड़-मरोड़ किये बिना क्या उनके युगन्धर रूप को देखा जा सकता है? क्या उनके स्वच्छ, नीलवर्ण जीवन-सरोवर का दर्शन किया जा सकता है? क्या ‘गीता’ में उन्होंने भिन्न-भिन्न योगों का मात्र निरूपण किया है? सच तो यह है कि श्रीकृष्ण के जीवन-सरोवर पर छाये शैवाल को तार्किक सजगता से हटाने पर ही उनके युगन्धर रूप के दर्शन हो सकते हैं।
प्रस्तुत है शिवाजी सावन्त के इस प्रसिद्ध उपन्यास का नवीनतम संस्करण।
ISBN: 978-81-263-1718-9
युगन्धर
श्रीकृष्ण-चरित्र पर केन्द्रित उपन्यास
प्रकाशक/लेखक की अनुमति के बिना इस पुस्तक को या इसके किसी अंश को
संक्षिप्त, परिवर्धित कर प्रकाशित करना या फ़िल्म आदि बनाना कानूनी अपराध है।
राष्ट्रभारती/लोकोदय ग्रन्थमाला: ग्रन्थांक 688
ISBN 978-93-263-5146-1
पहला संस्करण
: 2002
पाँचवाँ संस्करण
: 2005
नौवाँ संस्करण
: 2008
ग्यारहवाँ संस्करण
: 2010
बारहवाँ संस्करण
: 2012
तेरहवाँ संस्करण
: 2013
चौदहवाँ संस्करण
: 2014
पन्द्रहवाँ संस्करण
: 2015
सोलहवाँ संस्करण
: 2015
सत्रहवाँ संस्करण
: 2016
प्रकाशक:
भारतीय ज्ञानपीठ
18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003
आवरण: अनिल उपळेकर
आवरण-सज्जा: ज्ञानपीठ कला प्रभाग
सत्रहवाँ संस्करण: 2016
© अमिताभ एस. सावन्त
YUGANDHAR
(Marathi Novel)
by Shivaji Sawant
Published by
Bharatiya Jnanpith
18, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi-110 003
Ph.: 011 24698417, 24626467; 23241619 (Daryaganj)
Mob.: 9350536020; e-mail: [email protected]
[email protected], website: www.jnanpith.net
Seventeenth Edition: 2016
समर्पण
–जिस के लिए–‘तुम न होती तो?’ यह एक ही प्रश्न है मेरे ‘होने’ का–मेरे अस्तितव का निर्विवाद उत्तर, और विपरीत स्थितियों में भी जिसने कर्तव्य-तत्पर होकर ज्येष्ठ बन्धु श्री विश्वासराव की मदद से मंगेश, तानाजी और मैं–हम तीनों भाइयों के जीवन को आकार दिया, और इसके लिए हँसमुख रहकर कष्टसाध्य परिश्रम करते हुए जिसके पाँवों में छाले पड़ गये–अपनी उस (स्व.) मातुश्री राधाबाई गोविन्दराव सावन्त के वन्दनीय चरणों को स्मरण करके;
–और मराठी के ख्यातश्रेयस, साक्षेपी, ज्येष्ठ बन्धुतुल्य प्रकाशक श्री अनन्तराव कुलकर्णी, उनके सुपुत्र अनिरुद्ध रत्नाकर तथा समस्त कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन परिवार का स्मरण करके;
–और जिसने यह प्रदीर्घ रचना श्रीकृष्ण-प्रेम के कारण अथक निष्ठा से लिपिबद्ध की, जिसने प्रिय कन्या सौ. कादम्बिनी पराग धारप और चि. अमिताभ को अच्छे संस्कार दिये, जो मेरे लिए पहली परछाईं और मेरा दूसरा श्वास ही है–अपनी पत्नी सौ. मृणालिनी अर्थात् कुन्दा को साक्षी रख के;
–सभी पाठकों के साथ-साथ उसे भी प्रिय लगे ऐसे शब्दों में कहता हूँ – श्रीकृष्णार्पणमस्तु!
–शिवाजी सावन्त
आचमन
‘युगन्धर’ की मूल मराठी कथा शब्दांकित हुई। एक अननुभूत कार्यपूर्ति के अवर्णनीय आनन्द से मेरा मन लबालब भर आया है। अज्ञात मन की गहराइयों से मुझे तीव्रता से प्रतीत हो रहा है कि अब अपने मनोभाव को व्यक्त करने हेतु भी लेखनी न उठाऊँ। जो भी कहना है वह हजारों वर्षों से मर्मज्ञ भारतीयों के मन पर राज करता आया वह साँवला कान्हा ही अपने वर्ण के अनुसार गहरे, लहलहाते शब्दों में मुक्त मन से कहे। और इस कथा को ‘श्रीकृष्णार्पण’ कर, पिछले तीस वर्षों से कृष्ण को जानने के प्रयास में श्रान्त हुए अपने मन और शरीर को अब मैं विश्राम दूँ।
इस प्राक्कथन को मैंने ‘आचमन’ क्यों कहा है, यह बताना आवश्यक है। ‘आचमन’ अर्थात् समष्टि के हित-कल्याण हेतु परमशक्ति को मन-ही-मन आवाहन कर प्राशन की जलांजलि। ‘युगन्धर’ पढ़कर पाठक को इसकी प्रतीति अवश्य होगी, इस बात का श्रीकृष्ण-कृपा से मुझे पूरा विश्वास है। अत: प्रकट-अप्रकट शब्दों में व्यक्त किये इस मनोगत को मैंने ‘आचमन’ कहा है।
कुछ श्रद्धेय सुहृदों के तीव्र स्मरण से मेरी लेखनी स्तब्ध-सी हो गयी है–जिन्होंने आत्मीयता से युगन्धर की रचना की प्रगति के विषय में मुझसे बार-बार पूछताछ की थी। किन्तु उनके ‘युगन्धर कब पूर्ण होगा?’ इस प्रश्न का उत्तर स्वयं मुझे ही पता नहीं था, अत: देहू गाँव के सन्त तुकाराम महाराज की भाँति मन-ही-मन मेरा अपने-आप ही से संवाद होता रहता था। इस संवाद का कोई अन्त ही नहीं होता था। इसलिए केवल मुस्कराकर उस समय मैं मौन धारण कर लेता था। इन सुहृदों को झूठमूठ का आश्वासन देने का साहस मुझमें नहीं था। इनमें से दो तो ऐसे थे, जिनकी नस-नस में साहित्य और मानवता का प्रेम निरन्तर बहता रहता था।
इनमें पहले थे ऋषितुल्य–श्रद्धेय तात्यासाहेब–दूर-दूर तक फैले साहित्य-रसिकों के कण्ठमणि, कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज अर्थात् वि.वा. शिरवाडकर! और दूसरे थे पुणे के कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन के संचालक अनन्तराव कुलकर्णी अर्थात् भैयासाहेब!
मैंने अपनी पद्धति से ‘युगन्धर’ के व्यक्तित्व का अध्ययन पूर्ण किया। श्रीकृष्ण-जीवन से सम्बद्ध मथुरा, उज्जैन, जयपुर, कुरुक्षेत्र, प्रभास, द्वारिका, सुदामापुरी, करवीर आदि स्थानों की मैंने अन्वेषक यात्रा भी की। इस विषय से संलग्न कुछ विशेष विद्वानों से मैंने मुलाकातें भी कीं। कथावस्तु में सीधे प्रवेश करने के लिए मेरा मन मचलने लगा। मन की इसी स्थिति में मुझे नासिक शहर से व्याख्यानमाला का एक आमन्त्रण मिला। मैंने भी आदरणीय कुसुमाग्रज जी से भेंट करने की इच्छा से उसे स्वीकार किया।
‘आकृतिबन्ध’ (Form) की समस्या उनके आगे रखते हुए मैंने कहा, “सोच रहा हूँ कि श्रीकृष्ण द्वारा आत्मचरित्र कथन की शैली में उपन्यास की रचना करूँ!” निष्पाप बालक की भाँति कुसुमाग्रज जी मुस्कराये। ‘श्रीऽराम’ नाम लेकर बोले, “अच्छा विचार है। शीघ्र आरम्भ कीजिए।”
मन में निश्चय कर मैं पुणे लौट आया। संयोग से उसी समय हरिद्वार के रामकृष्ण सेवाश्रम के पूज्य स्वामीजी–अकामानन्द महाराज अनपेक्षितत: अपने शिष्य डॉ. इनामदार के साथ मेरे घर आये। उनको देखते ही मेरे मन में आया ‘इस प्रदीर्घ रचना का शुभारम्भ स्वामीजी के ही हाथों गन्ध-पुष्प अर्पित कर, शुभकर स्वस्तिकांकन करवा के क्यों न किया जाए?’ स्वामीजी ने भी प्रसन्नतापूर्वक सम्मति दी। उनके हाथों घरेलू पद्धति से पूजन करवाकर मैंने नम्रता से उनके चरणों पर माथा रखा। अपना स्नेहशील हाथ मेरी पीठ पर रखकर स्वामीजी ने अत्यन्त प्रेम से कहा, ‘तथास्तु–शुभं भवतु।’
श्रीकृष्ण के पहले ही शुभ अध्याय का इस प्रकार अनपेक्षित प्रारम्भ हुआ। लेखनिका श्रीमती सुधाजी लेले प्रतिदिन हमारे घर आने लगीं। श्रीकृष्ण के प्रदीर्घ कथन के दो सौ पृष्ठ पूरे हुए।
स्वामीजी फिर जब किसी काम से पुणे आये, मैंने अपना लेखन उनको पढ़कर सुनाया। गीता के गहरे अध्ययन के कारण स्वामीजी परम श्रीकृष्ण-भक्त हैं। वैज्ञानिक दृष्टि के कारण उनकी श्रीकृष्ण-भक्ति सजग है।
श्रीकृष्ण के जीवन के अधिकतर चमत्कारों को कठोरता से परे रखकर जीवन-कार्य की वास्तविकता को जान लेने का मेरा साहित्यिक व्रत उनको स्पर्श कर गया। मेरा लेखन उनको मनःपूर्वक भा गया। घण्टा-भर हम दोनों श्रीकृष्ण-चर्चा में ही मग्न रहे।
लेखन फिर शुरू हो गया। किन्तु मुझे तीव्रता से आभास होने लगा–अकेला श्रीकृष्ण ही अपनी पूरी जीवनगाथा सुनाए, यह ‘गीता’ के सन्दर्भ में भी उचित नहीं होगा। मैं फिर रुक गया–कई महीने तक मैं रुका ही रहा। जितना भी लेखन हो चुका था, मैंने सुधाजी से उसे फिर निर्दोष रूप में लिखवाया। उन्होंने भी कभी टालमटोल नहीं की।
मेरे मराठी प्रकाशक अनन्तराव जी आत्मीयता से मेरे पीछे पड़े थे–‘कब दे रहे हो मुझे ‘युगन्धर’?’
मैं तो भूमिका बाँधने में ही बहुत समय गँवा बैठा था। ऐसे में मुझे व्याख्यान के लिए नासिक जाने का अवसर फिर से प्राप्त हुआ। उस रामतीर्थ क्षेत्र में पहुँचते ही सबसे पहले मैं बन्धुतुल्य, साहित्य-अश्वत्थ कुसुमाग्रज जी से मिलने गया।
मैं उनके चरणस्पर्श कर ही रहा था कि मेरी भुजाओं को पकड़कर मुझे ऊपर उठाते हुए उन्होंने मुझसे वही प्रश्न पूछा, जिसका मुझे डर था–“पहले बताइए, क्या कहता है ‘युगन्धर’?’
नित्य की भाँति उन्होंने “कहाँ तक पहुँचा है ‘युगन्धर’?” नहीं पूछा था। उनकी बातों की दो पंक्तियों के बीच का आशय जानने का अब तक मुझे अच्छी तरह अभ्यास हो गया।
मैं निरुत्तर-स्तब्ध रह गया–कुछ क्षण ऐसे ही बीत गये। कुछ देर बाद मानो वे अपने-आप ही से बोले–‘मुश्किल क्या है? वैसे वह मुश्किल में डालनेवाला है ही–केवल यमुना-तट की ग्वालिनों को ही नहीं–उसे जानने का प्रयास करनेवाले को भी!”
मैंने फिर से ‘शैली’ की मुश्किल बतायी। उन्होंने निरागस मुस्कराते हुए कहा, “ ‘मृत्युंजय’ की शैली में क्या बुराई है?” उनके स्वभाव के अनुसार यह सूचनात्मक सलाह ही थी। कुछ समय सोचकर मैंने कहा, “पाठकों को वह ‘मृत्युंजय’ की शैली का अनुसरण लगेगा।”
“बिलकुल नहीं। इसी शैली में महाभारत के विषय पर आप और भी दस उपन्यास लिख सकते हैं। प्रश्न यह है कि उस व्यक्तित्व का आप कहाँ तक आकलन कर सके हैं! अब रुकिये मत। ‘मृत्युंजय’ की ही शैली में आप ‘युगन्धर’ को पूरा कीजिए।”
मैं चुप हो गया। कितना तर्कसंगत सुझाव दिया था तात्यासाहेब ने! प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण ने अर्जुन को एक विशेष अवसर पर ‘यह है सूर्य और यह जयद्रथ’ का सीधा संकेत दिया था। (मैं अर्जुन नहीं हूँ, यह मैं जानता हूँ, किन्तु श्री. वि. वा. शिरवाडकर अर्थात् कुसुमाग्रज जी मराठी की साहित्य-द्वारिका के द्वारिकाधीश हैं, यह ध्यान में रखते हुए) उनकी सलाह मुझे आज्ञा जैसी लगी।
नासिक से लौटते हुए मन-ही-मन मैं छानने लगा, “ ‘युगन्धर’ में किस-किस व्यक्तित्व को मुखर करना होगा! महाभारत के सशक्त मेरुदण्ड श्रीकृष्ण के जीवन में शब्दश: हजारों स्त्री-पुरुष आये थे। उनमें से किसको चुनना है और किसको छोड़ना है! क्यों? कैसे? कौन-सी कसौटी पर?” मेरे मन में प्रश्नों का प्रचण्ड महाभारत शुरू हुआ।
अन्वेषण श्रीकृष्ण का करना था–एक बहुआयामी, प्रत्येक श्वास के साथ प्रतीत होनेवाले प्रिय व्यक्तित्व का, क्षण-भर में सुनील नभ को व्याप्त कर, दूसरे ही क्षण गहरे काले अवकाश के उस पार जानेवाले, भार रहित ब्रह्माण्ड को व्याप्त करनेवाले एक ऊर्जा-केन्द्र के भी केन्द्र, मोरपंखी, कालजयी, अजर व्यक्तित्व का था यह अन्वेषण!
जैसे-जैसे मैं अधिकाधिक चिन्तन की गहराई में उतरता गया, मुझे तीव्रता से स्पष्ट होता गया कि कदाचित् श्रीकृष्ण को उसके अधिक-से-अधिक आयामों सहित जीवन की विविध छटाओं सहित जान लेना सम्भव होगा, किन्तु उसे औरों को समझाना–वह भी ललित साहित्य के माध्यम से–अत्यन्त कठिन है।
ऐसा क्यों होता है कि श्रीकृष्ण अधिक-से-अधिक निकट भी लगता है और बात-बात में वह कहीं दूर–क्षितिज के उस पार भी जा बैठता है। मन को वह एक अनामिक, अनाकलनीय व्याकुलता क्यों दे जाता है? इसे खोजने की धुन मुझ पर सवार हो गयी। इसलिए प्राणायाम पर आधारित साधना मैंने प्रारम्भ की।
तब पहली ही बात मुझे प्रतीत हुई कि श्रीकृष्ण का हम सबके अन्दर अंशत: वास होते हुए भी हमें उसका आभास नहीं होता है। इसका कारण यह है कि पिछले पाँच हजार वर्षों से वह एक से बढ़कर एक चमत्कारों में अन्तर्बाह्य लिप्त हो गया है। अन्धश्रद्धाओं के जाल में फँसा हुआ है।
उसके विराट् रूपधारी, सहस्रों हाथों-मुखोंवाले रूप की कल्पना कर, महाभारत ने जो हजारों वर्षों की यात्रा की है, अनेक प्रज्ञावान महाकवियों ने उसमें अपनी दीप्तिमान प्रतिभा की तेजस्वी समिधाएँ अर्पित कर उसको सामान्य जनों से कोट्यवधि योजन दूर लाकर खड़ा किया है। यह सब उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। उनके निर्मल परन्तु भोले-भाले, सरस भक्तिभाव के कारण उनके हाथों यह स्वाभाविकत:, अपने-आप ही घटित हुआ। वैसे देखा जाए तो अर्वाचीन इतिहास में अपने सभी साथियों और पालतू प्राणियों सहित औरंगजेब की कैद से, आगरा से बड़ी कुशलता से भाग खड़े होनेवाले शिवाजी महाराज को भी तत्कालीन समाज ने आदरपूर्वक शिव का अवतार माना था।
साधनामग्न, अलिप्त मन को ‘युगन्धर’ का पहला ही अत्यन्त अनमोल साहित्य-सत्य स्पर्श कर गया। विज्ञान युग के शिखर पर पहुँची इस सदी के अन्तिम विशिष्ट मोड़ पर खड़े रहकर श्रीकृष्ण को जानने के लिए, उसके चरित्र पर भावुकता से चढ़ाई गयी चमत्कार की पर्तों को निश्चयपूर्वक दूर हटाना होगा। यही काम बड़ा कठिन था।
भारताचार्य चिं. वि. वैद्य जैसे अध्ययनशील, तज्ज्ञ भाष्यकार ने श्रीकृष्ण का जीवनकाल एक-सौ-एक वर्षों का बताया है। क्या यह सम्भव है? (आजकल के प्रदूषित वातावरण की मानवीय आयुर्मर्यादा की कसौटी पर परखने की भूल न करते हुए) हाँ–यह सम्भव है, यही इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है।
श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उसके प्रदीर्घ जीवन में ऐसा एक भी क्षण व्यतीत नहीं हुआ, जब कुछ-न-कुछ घटित न हुआ हो। श्रीकृष्ण सभी अर्थों में जीवन को गढ़नेवाली महान विभूति है। उसका सबसे बड़ा गुणधर्म यही है कि जहाँ-जहाँ जीवन को बिगाड़नेवाली दुष्ट, अमंगल शक्तियाँ जीवन के मार्ग में रुकावट बनकर खड़ी हुईं, दूरदर्शिता से पहले ही उन्हें पहचानकर श्रीकृष्ण ने भिन्न-भिन्न मार्गों से उन्हें अविलम्ब जड़ सहित उखाड़ दिया। भारतीय जनगंगा का जीवन-मार्ग सदा के लिए कण्टकमुक्त किया।
उन दुष्ट शक्तियों का निर्दलन करते हुए श्रीकृष्ण ने हर बार अपने चकित कर देनेवाले पौरुष का अकल्पित-सा कार्य दिखाया। प्रत्येक प्रसंग में उसने एक ही शस्त्र, एक ही उपाय का नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार अलग-अलग उपाय का प्रयोग किया। क्या इसी से ही उसका अपने पूर्व के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक–सम्पूर्ण भारतीय जीवन को मोड़ देनेवाला ‘युगन्धर’ रूप उद्घाटित नहीं होता?
क्या जीवन के मूलभूत लक्षण–वृद्धि और विकास–के आड़े आनेवाली अ-शिव शक्तियों का केवल निर्दलन करना ही जीवन को गढ़ना होता है? नहीं! यह तो जीवन का नकारात्मक दृष्टिकोण होगा। जीवन को गढ़नेवाली जिस सकारात्मक दृष्टि को श्रीकृष्ण ने अपनाया और जिस सजगता से स्थान-स्थान पर उसका उपयोग किया, एक साहित्यिक के नाते इस ज्ञान-विज्ञान-प्रज्ञान के चैतन्यमय युग में मुझे वह अत्यन्त अनमोल लगती है।
अपने जीवन में आये शब्दश: सहस्रों नर-नारियों से उसने विशुद्ध प्रेमभाव का ही आचरण किया। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीकृष्ण कभी कालबाह्य नहीं होगा।
श्रीकृष्ण-चरित्र का अध्ययन करते हुए मुझे तीव्रता से प्रतीत हुआ कि उपनिषद् काल से, पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रवाहित होता आया, सूर्य-किरणों के समान शाश्वत सत्य–‘न हि मनुष्यात् श्रेष्ठतरं किंचित्–’ जिसे श्रीकृष्ण ने सभी आयामों से जान लिया, उसे श्रीकृष्ण के पूर्व इस देश में किसी ने नहीं जाना। विचार के इस धागे के साथ चलते-चलते एक महत्त्वपूर्ण बात मेरे ध्यान में आयी। श्रीकृष्ण-चरित्र में केवल गीता को हमने वैश्विक तत्त्वज्ञान के अत्युच्च आविष्कार के रूप में स्वीकार किया। पीढ़ियों से हम उसे बिना समझे केवल रटते रहे।
नि:सन्देह गीता तत्त्वज्ञान का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है। इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता–मेरा तो है नहीं। किन्तु पूर्ण अध्ययन के बाद मैं समझ-बूझ के साथ विधान कर रहा हूँ कि ‘उसके प्रत्येक चरण-चिह्न के साथ जो अनुभव-गीता अंकित होती गयी, उसकी हमने उपेक्षा की! वह भी उसी की भरतभूमि में जन्म लेकर!’
उदाहारण के लिए मैं दो बातें बताना चाहूँगा। श्रीकृष्ण की आठ रानियों में से एक आदिवासी थी–ऋक्षवान पर्वत के आदिवासी राजा जाम्बवान की कन्या–जाम्बवती!
पूर्ण अध्ययन और चिन्तन के पश्चात् उसके ‘युगन्धर’ चरित्र को सामने रखते हुए मैं विधान करता हूँ कि उसके पहले किसी भी क्षत्रिय अथवा उच्च वर्ण के व्यक्ति ने जीवन-गंगा को आमूल मोड़ देने का ऐसा आदर्श कर्म नहीं किया है। श्रीकृष्ण को ‘युगन्धर’ के रूप में स्वीकृत करने के लिए कभी हमने इस सत्य पर तनिक भी विचार किया है?
इसी समय यह भी कहना आवश्यक है कि अच्छे-अच्छों ने सर्वाधिक कठोरता से अकेले श्रीकृष्ण की कड़ी आलोचना की है–वह भी गीता के एक श्लोक–‘चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम्’ के आधार पर!
सबसे पहले यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि महाभारत कोई झूठमूठ की कहानी नहीं है। वह भारतवर्ष का प्राचीनतम उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज है–किन्तु उस पर प्रक्षेपों की पर्तें-ही-पर्तें चढ़ी हुई हैं।
अठारह पर्वों और एक लक्ष श्लोकोंवाला प्रचलित महाभारत अनेक प्रज्ञावान ऋषियों की प्रक्षिप्त रचनाओं से लदी हुई संहिता है। मूलत: ‘भारत-सावित्री’ अथवा ‘जय नामक इतिहास’ नाम की यह वीरगाथा तेरह गुना बढ़ाकर अठारह पर्वों और एक लक्ष श्लोकों में विकसित हो गयी है। भारतीय जीवन-प्रणाली के मानक ग्रन्थ के रूप में यह ग्रन्थ आज विश्वमान्य हो गया है। उसमें से ‘गीता’ तत्त्वज्ञान के उपाख्यान का एक भाग है। ‘गीता’ महाभारत के कथासागर की ऐसी बहुमोल गागर है, जिसकी बूँद-बूँद में मानव-जीवन के सागर को मथ डालने की सामर्थ्य है। कौरव-पाण्डव और श्रीकृष्ण का सन्दर्भ ‘गीता’ में आवश्यकता के अनुसार ही आया है।
आदिवासी स्त्री (जाम्बवती) को ब्याहकर उसे पत्नी का गौरव दिलानेवाला एकमात्र कृष्ण ही है। राजसूय यज्ञ में वह आमन्त्रितों के जूठे पात्र उठाता है, अपने गरुड़ध्वज रथ के चारों अश्वों का खरहरा वह स्वयं करता है। सारथि दारुक को रथ के पार्श्वभाग में बिठाकर वह स्वयं गरुड़ध्वज का सारथ्य करता है।
जीवन में किसी भी कर्म को वह निषिद्ध नहीं मानता। तब वह कैसे कह सकता है कि ‘वर्णाश्रम का कर्ता मैं ही हूँ।’ इस सरल से तर्क को भी हमने हजारों वर्ष स्वीकार नहीं किया है। समझ में नहीं आता, किसी भी विचारक ने श्रीकृष्ण-जीवन के जाम्बवती की वास्तविकता को ध्यान में लेते हुए यह प्रश्न कभी क्यों नहीं उठाया!
निर्धन सुदामा से श्रीकृष्ण का निरपेक्ष स्नेह, सारथि दारुक के लिए उसका मनोभाव, गोकुल के गोपालों के साथ उसका सख्य निर्मल मन से देखनेवाला कौन अभ्यासक उसको ‘वर्णनिर्माता’ कह सकता है! इसके लिए विद्वानों को ‘गुणकर्म’ की कृतक ढाल के पीछे छिपने की आवश्यकता ही क्या है?
मेरे चिन्तन की छलनी से ऐसे कई प्रखर सत्य मुझे श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में स्पष्ट दिखाई दिये। उन सभी सत्यों को मैंने इस प्रदीर्घ रचना में यथाशक्ति स्पर्श किया है।
श्रीकृष्ण के कई सखा हैं–पेंधा सहित सभी गोपाल, बलराम, सुदामा, दारुक, सात्यकि, अर्जुन, महात्मा विदुर, भीष्म आदि। उसका ककेरा बन्धु उद्धव उसका परम सखा है। ‘गीता’ के बाद केवल उसके लिए श्रीकृष्ण ने ‘उद्धवगीता’ निरूपित की। महाभारतीय युद्ध के पश्चात् अकेले उद्धव की सेवा को श्रीकृष्ण ने अन्त तक स्वीकार किया। ‘ऐसा क्यों?’ यह प्रश्न आज तक किसी के मन में नहीं उभरा।
इसका स्पष्ट अर्थ है कि उद्धव श्रीकृष्ण का केवल ककेरा बन्धु अथवा प्रिय यादव होने के नाते उसका सखा नहीं है। वह उसका भावविश्वस्त है। जिस प्रकार ‘रामायण’ में श्रीराम का भावविश्वस्त भरत था उसी प्रकार अथवा उससे भी बढ़कर श्रीकृष्ण-जीवन में उद्धव श्रीकृष्ण का भावविश्वस्त था, यह सत्य मुझे अपने चिन्तन में सर्वाधिक स्पर्श कर गया।
नायक श्रीकृष्ण के विषय में मैंने बार-बार बहुत-कुछ कहा है, बहुत से लेख लिखे हैं। किन्तु यहाँ मैं श्रीकृष्ण के केवल ‘श्री’ विशेषण के विषय में, उसके ‘जलपुरुषत्व’ के विषय में और उसके अन्य दो जलपुरुषों के साथ भावसम्बन्धों के विषय में विमर्श करना चाहूँगा। हीरे की भाँति संस्कृत के सम्मानसूचक ‘श्री’ शब्द के कई पहलू हैं–कई अर्थ हैं। ‘श्री’ अर्थात् सौन्दर्य, ‘श्री’ अर्थात् अनिरुद्ध सामर्थ्य, अलौकिक बुद्धि, अपार सम्पत्ति, असीम गुणवत्ता आदि। कोई भी परिश्रमशील अभ्यासक श्रीमद्भागवत, महाभारत, हरिवंशपुराण आदि पुराणों में ‘कृष्ण’ को खोज सकते हैं। किन्तु ‘श्री’ से युक्त कृष्ण को खोजने के लिए और उसे औरों को समझाने के लिए ललित-लेखक की ही आवश्यकता है, यह मेरा नम्र किन्तु निश्चित कथन है।
महाकाव्य रामायण का नायक राम अपने गुणों के बल पर ‘श्रीराम’ बना। उसी प्रकार महाभारत का नायक कृष्ण अपनी गुणवत्ता से ‘श्रीकृष्ण’ बना। इन दोनों महाकाव्यों में भूलकर भी अन्य किसी को ‘श्री’ की उपाधि लगाकर श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत अथवा श्रीभीम, श्रीअर्जुन नहीं कहा गया है।
क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि श्रीकृष्ण में वास करनेवाला ‘श्री’ पहले रचनाकार को प्रतीत होना आवश्यक है। फिर वीणावादिनी ज्ञानदेवी सरस्वती की रक्तिम करांगुलि का स्पर्श यदि उसकी प्रतिभा को हो जाए, तब सम्भवत: वह अपने नायक को शब्दों में उद्घाटित कर पाएगा। मुझे विश्वास है कि अब महाभारतीय व्यक्तिरेखाओं के आकलन में प्रगल्भ हुए पाठकों को ‘युगन्धर’ के प्रत्येक प्रसंग में दो पंक्तियों के बीच अप्रकट किन्तु निःसन्देह वास करनेवाला ‘श्री’ अचूक स्पर्श कर जाएगा।
इस चिन्तन में एक नया ही लोमहर्षक आकलन मुझे छू गया। श्रीकृष्ण, भीष्म और कर्ण पंचमहाभूतों में से महत्त्वपूर्ण जलतत्त्व की व्यक्तिरेखाएँ हैं। मूलत: ये तीनों ‘जलपुरुष’ हैं। जब कभी वे आपस में मिलते हैं, एक-दूसरे का मौन आदर करते हैं। जन्मत: पिता के मस्तक पर से, यमुना के जलप्लावन से जीवन-यात्रा का आरम्भ करनेवाला श्रीकृष्ण, उसी प्रकार जन्म लेते ही अश्वनदी, चर्मण्वती, गंगा–इन नदियों में से बहते हुए अपनी कठिन जीवन-यात्रा का आरम्भ करनेवाला–कुमारी कुन्ती माता का त्यागा कर्ण और प्रत्यक्ष जलमाता–गंगा के पुत्र–गांगेय भीष्म! इनके सुप्त, अज्ञात मन के ‘जलपुरुष’ के नाते के साथ-साथ चलते हुए हम इन तीनों महान व्यक्तिरेखाओं के सीधे मर्मस्थल तक पहुँच सकते हैं–यह मेरा अनुभव है। तब ये तीनों व्यक्तिरेखाएँ अन्तर्बाह्य अलग ही प्रकट होने लगती हैं। एकदम अलग भाषा में वे रचनाकार से संवाद करने लगती हैं।
इसीलिए ‘युगन्धर’ के नीलवर्णी सखा श्रीकृष्ण और अर्जुन को भी पाठक सूक्ष्मता से पढ़ें।
श्रीकृष्ण के सखा अनेक, गुरु दो, बहनें तीन, दो माता-पिता, आठ पत्नियाँ, अस्सी पुत्र और चार पुत्रियाँ थीं–किन्तु सखियाँ दो ही थीं–पहली राधा और दूसरी द्रौपदी।
लोकमानस में जिसकी जड़ें जमी हुई हैं, उस राधा का श्रीकृष्ण से सम्बन्ध का भागवत, महाभारत, हरिवंशपुराण आदि ग्रन्थों में कहीं भी स्पष्ट निर्देश तक नहीं है।
‘राधा’ का ‘युगन्धर’ में क्या किया जाए? राधा की व्यक्तिरेखा श्रीकृष्ण-चरित्र से कब चिपक गयी? कैसे? पन्द्रहवीं सदी में कवि जयदेव के अत्यन्त जनप्रिय, शृंगाररस प्रधान रसीले खण्डकाव्य ‘गीतगोविन्द’ से उसने श्रीकृष्ण-चरित्र में प्रवेश किया। तत्पश्चात् ‘गीतगोविन्द’ को आधार बनाकर प्रतिभावान कवियों ने राधा की व्यक्तिरेखा को मनःपूत भिन्न-भिन्न आविष्कारों में श्रीकृष्ण के साथ अपनी-अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया।
राधा का दामन थामकर काव्य-क्षेत्र में रसिक कृष्ण ने सदियों तक असमर्थनीय ऊधम मचाया। वास्तव में जीवन में नारी का आदर करनेवाला श्रीकृष्ण काव्यों में स्त्रीलोलुपता की ओर घसीटा गया।
बहुत सोचने के बाद मैंने ‘राधा’ को अपने उपन्यास में स्थान न देने का पक्का निर्णय किया।
चिन्तन के गुत्थमगुत्थे में ही प्रकाश-किरण की तरह एक विचार मेरे मन में आया–सदियों से भक्तजन ‘राधे-कृष्ण’ का जयघोष करते आये हैं–उस ‘राधा’ शब्द का अर्थ वस्तुत: क्या है?
बड़ी खोजबीन के बाद ‘राधा’ शब्द का जो अर्थ मुझे मिला। उससे मेरे अन्दर का साहित्यकार रोमांचित हो उठा–आज भी मैं उस क्षण को भूल नहीं पाता।
राधा संयुक्त शब्द है– रा + धा – ‘रा’ का अर्थ है ‘प्राप्त हो’ और ‘धा’ का अर्थ है ‘मोक्ष…मुक्ति’।
‘राधा’ अर्थात् मोक्षप्राप्ति के लिए व्याकुल जीव! इस शब्दार्थ से मेरा सम्पूर्ण चिन्तन मूल से आलोड़ित हो उठा। अपने लेखन से हटायी राधा अपने-आप प्रबल आवेग से मेरे मन की गुफा में प्रवेश करने लगी। गोकुल की प्रत्येक गोपी में मुझे राधा का प्रत्यय होने लगा। ‘राधा’ मोक्षप्राप्ति के लिए व्याकुल जीव! हर गोपी राधा! हर राधा व्याकुल मोक्षार्थी! वे सब-के-सब मोक्षप्राप्ति के लिए व्याकुल जीव तो थे! मैंने मन-ही-मन निश्चय कर लिया–राधा को प्रतिनिधिक गोप-नारी के रूप में लेना अति आवश्यक है। श्रीकृष्ण-कथा में राधा अनिवार्य है–किन्तु उसका चित्रण सावधानी से, संयम से होना चाहिए–विचारपूर्वक मैंने ऐसा ही किया।
श्रीकृष्ण की दो ही बहनें मानी गयी हैं–सुभद्रा और मानस भगिनी द्रौपदी। किन्तु उसकी तीसरी भी एक बहन है, जो अनुल्लेख के घने अँधेरे में छिपी हुई है। वह है नन्द-यशोदा की पुत्री एकानंगा–कृष्ण की गोपभगिनी–‘एका’। यहाँ उसे सीमित परन्तु उचित साहित्यिक दृष्टि से लिया गया है।
श्रीकृष्ण के गुरु भी दो हैं–पहले गुरु आचार्य सान्दीपनि तो सर्वज्ञात हैं। आश्रम शिष्य–युगन्धर श्रीकृष्ण का अवन्ती के अंकपाद आश्रम का जीवन पहली ही बार प्रत्ययकारी और चित्रदर्शी शैली में प्रस्तुत हुआ है या नहीं यह तो पाठकों को ही तय करना है। जग को ललामभूत, श्रीकृष्ण का अमर, कालजयी तत्त्वज्ञान का ग्रन्थ–गीता, जिनकी ब्रह्मविद्या की सीख से साकार हुआ, वे श्रीकृष्ण के दूसरे गुरु हैं आचार्य घोर-आंगिरस। उनकी सभी जीवन-छटाओं सहित यहाँ वे पहली बार पाठकों से बात करेंगे, इसका मुझे विश्वास है।
इस कथावस्तु में ऊपर-ऊपर सामान्य लगनेवाली दो व्यक्तिरेखाएँ हैं–दारुक और सात्यकि। पहला है श्रीकृष्ण के गरुड़ध्वज रथ का उसके महानिर्वाण तक सारथ्य करनेवाला उसका आज्ञाकारी, चतुर, कुशल सारथि। स्वयं श्रीकृष्ण सारथियों का भी सारथि है। इसमें लक्षणार्थ अत्यन्त मार्मिक है। वह विचार-रथ का सारथ्य करनेवाला है। वह विचारकों का भी विचारक है। इसलिए वह किशन, कन्हैया, गोपाल, गोविन्द, मोहन, कृष्ण, दामोदर, मुरलीधर, श्याम, मधुसूदन, माधव, मिलिन्द, श्रीकृष्ण, अच्युत, द्वारिकाधीश, वासुदेव जैसे एक से बढ़कर एक विशेष गुणयुक्त नामों से विश्वविख्यात हुआ। ऐसे विचारवानों के विचारवान, सारथियों के सारथि का जीवन-भर सारथ्य करने का परम सौभाग्य दारुक को अन्त तक प्राप्त हुआ। दारुक रुक्मिणी से भी अधिक काल तक श्रीकृष्ण के सान्निध्य में रहनेवाली एकमात्र व्यक्तिरेखा है।
दारुक में मुझे एक सुप्त, प्रभावशाली व्यक्तिरेखा दिखाई दी। श्रीकृष्ण-चरित्र से सम्बद्ध सभी सन्दर्भ-ग्रन्थों में दारुक का केवल उल्लेख मिलता है। उसे मुखर करना मेरे अन्दर के सृजनशील लेखक को एक चुनौती ही प्रतीत हुई। उसी की तरह अबोल रहकर मैंने इसे स्वीकार किया। श्रीकृष्ण के चार दुग्ध-धवल, जीवनीशक्ति से भरपूर, पुष्ट अश्वों के साथ-साथ कृष्ण-सारथि दारुक ने अपनी ‘सारथि-गीता’ को यहाँ स्पष्ट कर दिखाया है अथवा नहीं, इसका निर्णय पाठक ही करें।
जो स्थिति दारुक की है, एक अलग प्रकार से वही स्थिति यादव-सेनापति सात्यकि की है। श्रीकृष्ण के बाद अकेले सात्यकि का ही ‘आजानुबाहु-महारथी’ के रूप में सन्दर्भ मिलता है। उसकी इसी विशेषता ने मुझे उसे ‘युगन्धर’ में मुखर करने पर विवश किया। श्रीकृष्ण ने जीवन-भर जिस बुद्धि-कौशल से उन्मत्त अत्याचारियों का सामना किया, उसी से वह जग में अजेय योद्धा सिद्ध हुआ। गीता के कारण वह सर्वश्रेष्ठ तत्त्वज्ञ प्रमाणित हुआ। मेरे चिन्तन में जब यह तत्त्वज्ञ-योद्धा (Philosopher-warrior) चलने लगता था, परछाईं की भाँति अर्जुन उसके पीछे-पीछे रहता था। किन्तु जब श्रीकृष्ण विश्राम करता था अथवा किसी मन्त्रणा-बैठक में होता था, युद्ध-सम्मुख यादवों का महापराक्रमी, अनुभवी, आजानुबाहु सेनापति सात्यकि उसकी परछाईं बन जाता था।
श्रीकृष्ण ने अपने वैवाहिक जीवन में अन्तःपुर में प्रिय पत्नी रुक्मिणी से यथेच्छ बातें कीं। सखी द्रौपदी से उसने स्त्रीत्व के जीवन-सत्य के विषय में संवाद किया। गरुड़ध्वज रथ में उसने सखा अर्जुन से वार्त्तालाप किया। कुरुक्षेत्र के शिविर में उसने आजानुबाहु सात्यकि से मनःपूर्वक मन्त्रणा की। किन्तु महाभारतीय युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वारिका लौटने पर महर्षि घोर-आंगिरस से भेंट और संवाद के बाद ढलती आयु में चिन्तनशील, व्रतस्थ बने–मन से वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार किये श्रीकृष्ण के द्वारिका के अन्तिम निवासकाल में उसका भावविश्वस्त बना अकेला उद्धव।
इस महाकथावस्तु में उद्धव मेरे साहित्यिक भावकेन्द्र से सर्वाधिक छू गयी रससम्पन्न व्यक्तिरेखा है। किसी बात को कोई समर्थन देने का दायित्व न लेनेवाली, श्रीकृष्ण के बाद मेरी प्रिय भाव-व्यक्तिरेखा यही है। जैसे श्रीकृष्ण और कर्ण एक ही मुद्रा के दो पहलू हैं, उसी प्रकार एक अलग, गहरे अर्थ में श्रीकृष्ण और उद्धव भी एक ही तात्त्विक मुद्रा के दो सशक्त पहलू हैं। यदि उद्धव अर्जुन की भाँति शस्त्र लेकर श्रीकृष्ण के साथ जीवन-संग्राम में उतरता तो? क्या वह भीष्म, बलराम, अर्जुन, कर्ण को पीछे छोड़ जाता? किसी भी आलोचक को अन्तर्मुख होकर सोचने पर बाध्य करनेवाला यह प्रश्न है।
जीवन में कभी किसी प्रकार का शस्त्र धारण न करनेवाले सुमित्र सुदामा को श्रीकृष्ण के विमल नेत्रों से झरे स्नेहल आत्मरस का अभिषेक अपने मस्तक पर धारण करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ–वह धन्य हो गया–सच्चा मित्र सिद्ध हुआ।
शस्त्र का कभी भी उपयोग न करनेवाला उद्धव भी श्रीकृष्ण का भावविश्वस्त बना। श्रीकृष्ण के निर्वाण के पश्चात् बदरी-केदार में उसके नाम पर आश्रम का निर्माण कर उद्धव कृतार्थ हुआ–अमर हुआ।
सुदामा और उद्धव दो छोर की व्यक्तिरेखाएँ हैं। गोकुल की गोपियाँ और श्रीकृष्ण की मुक्त और पुनर्वसित की हुई कामरूप की सोलह हजार नारियाँ भी स्त्री-जीवनसत्य के दो भिन्न-भिन्न छोर हैं। आचार्य सान्दीपनि और घोर-आंगिरस परमोच्च गुरु तत्त्व के दो छोर हैं। यादवश्रेष्ठ वसुदेव और गोपनायक नन्द दो छोर के वन्दनीय पितृस्थान हैं। जीवन में पराकोटि के भावाघात सहती रही माता देवकी और अन्तर्बाह्य निर्मल, भोले-भाले, प्रेमल गोप-गोपियों की निरलस माता यशोदा दो छोर के पूजनीय मातृस्थान हैं। गोप-सखी राधिका और पाण्डव-सखी द्रौपदी किसी भी लौकिक संकल्पना की पकड़ में न आनेवाली दो छोर की भाव-सखियाँ हैं।
इसके अतिरिक्त बलराम, रेवती, भीष्म, महात्मा विदुर, संजय, अर्जुन सहित सभी पाण्डव, कुन्ती बुआ, पांचाल-युवराज धृष्टद्युम्न और पांचाल, यादव, कौरव, पाण्डव, विराट आदि सहस्रों नर-नारियों ने जिसे वन्दनीय माना वह ‘वासुदेव’, योगयोगेश्वर, पूर्णरूप श्रीकृष्ण आज भी हमें ‘हृदयस्थ’ क्यों लगता है? विज्ञान कितनी भी उड़ान क्यों न भरे, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान को व्याप्त करके भी दशांगुल शेष रहनेवाला ‘श्री’ सदैव ही सबके मन में ताजा रहनेवाला है। उसके युगन्धरत्व को जानने का मैंने यथामति, यथाशक्ति प्रयत्न किया है।
सन्दर्भ-शोधन की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल और परिश्रमों की परीक्षा लेनेवाली, शब्दों की पकड़ में न आनेवाली, बालों के गुत्थे जैसी होती है। उसे समझने का प्रयास न करना ही उचित होगा। फिर भी सन्दर्भ-शोधन के लिए जब मैं पुणे में–भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट में आसन जमाये रहता था, वहाँ के डॉ. वा. ल. मंजुळ, डॉ. मेहेंदळे, डॉ. विजया देशमुख, श्री सतीश सांगले आदि सभी कर्मचारियों ने (तनिक भी नाराजगी न दिखाते हुए) प्रसन्न मुख और मन से लम्बे समय तक मेरी जो सहायता की है उसे मैं भूल नहीं सकता।
यह महाकाय रचना-कार्य कुछ वर्ष चलता रहा। इसकी पहली लेखनिका थीं श्रीमती सुधाजी लेले। पहले ही अध्याय के बाद कुछ घरेलू कठिनाइयों के कारण वे इस लेखन-कार्य से निवृत्त हो गयीं। लम्बे समय तक मेरा लेखन भी जहाँ का तहाँ रुक गया। फ़र्ग्युसन महाविद्यालय के प्राचार्य सन्मित्र श्री वसन्तराव जी वाघ ने इस काम के लिए कुछ विद्यार्थियों को मेरे पास भेज दिया। फिर भी लेखन अधूरा ही रहा। उन्होंने मेरी जो सहायता की उसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।
दो अध्यायों के बाद मेरा लेखन-कार्य रुक ही गया था। फिर एक दिन मेरे मित्र–श्री. एन. एस. राउत जी के सुझाव पर मेरी पत्नी–श्रीमती मृणालिनी मेरी लेखनिका बनी। उसके बाद हमारे लेखन ने गति पकड़ी। छह महीने तक हमारा काम समयबद्ध चलता रहा।
पुस्तक के मुकुटमणि अन्तिम अध्याय–‘उद्धव’ के लेखन में हम व्यस्त थे। दिसम्बर 1998 में मैं अचानक बीमार हो गया। मुझे श्वास लेने में दिक्कत होने लगी। मेरे साहित्यप्रेमी सुहृद डॉ. मदन जी फडणीस के कहने पर मैं हॉस्पिटल में भरती हुआ। मुझे हार्ट-अटैक हुआ था। तीन दिन मुझे आइ. सी. यू. में रहना पड़ा। अभी सौ पन्ने लिखना बाकी था। दस दिन हॉस्पिटल में रहकर मैं घर लौट आया। उसके बाद शीघ्र ही मैंने युगन्धर का लेखन पूर्ण किया और वह पाण्डुलिपि कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन के श्री रत्नाकर कुलकर्णी के हाथ सौंप ही दी।
इस हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन के लिए भारतीय ज्ञानपीठ को सानन्द सहमति देने के लिए, मूल मराठी प्रकाशक कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन का मैं हार्दिक आभारी हूँ।
मैं बस इतना ही मानता हूँ–यह श्रीकृष्णलीला है। उसे पूर्णत: जान पाना क्या कभी किसी के लिए सम्भव होगा?
अन्तत: गीता के अर्थपूर्ण शब्दों में इतना ही कहता हूँ–
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।।
यह आचमन करने से पूर्व केवल मुझे ही नहीं, जो हर किसी को कहना होगा, वही मैं कहता हूँ–श्रीकृष्णार्पणमस्तु!
–शिवाजी सावन्त
3-रा. प. हाउसिंग सोसायटी
पर्वती ब्रिज के पास, सिंहगढ़ रस्ता
पुणे – 411 030
दूरध्वनि : 433 5655
कृतज्ञता
‘युगन्धर’ के अनुवाद के समय जिन्होंने किसी-न-किसी रूप में मेरी सहायता की है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य है।
सबसे पहले मैं कृतज्ञ हूँ अपने पति श्री शिवाजी सावन्त और पुत्र अमिताभ की। मेरे लेखन-काल में इन दोनों ने गृहकर्मों से मुझे छूट दी, इसलिए मैं इतना बड़ा काम कर सकी।
मेरे अनुवाद-कार्य के संशोधन में डॉ. केशव प्रथमवीर ने मेरी अमूल्य सहायता की है, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं।
मेरी बहनों–श्रीमती अनुराधा, मानसी और वृषाली तथा बहनोई श्री अजितराव वैद्य, पद्माकर देवधर और किरण फडके तथा उनकी बेटियाँ कु. मिनू, चैत्रू, श्वेता और उर्विजा–इन सबकी सहायता के बिना कुछ कर पाना मेरे लिए असम्भव था। मेरा अनुवाद-कार्य पूरा होने तक इन सबने अत्यन्त आत्मीयता से, स्नेह से मेरा जो खयाल रखा है, उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के बदले मैं निरन्तर उनके स्नेहबन्धन में रहना ही पसन्द करूँगी।
मैं मानती हूँ कि युगन्धर–श्रीकृष्ण ने ही इन सबको–स्वयं मुझे भी–इस कार्य के लिए प्रेरित किया था। उसी के चरणों में मेरे द्वारा अनूदित यह पहली कृति नम्रतापूर्वक अर्पित है। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
–मृणालिनी सावन्त
पुणे
26 जनवरी, 2002
अनुक्रम
श्रीकृष्ण
रुक्मिणी
दारुक
द्रौपदी
अर्जुन
सात्यकि
उद्धव
श्रीकृष्ण
आज मुझे कुछ कहना ही होगा! चौंकिए मत, घबराइए भी नहीं। दौत्य करनेवाले श्रेष्ठ, सम्भाषण-चतुर वक्ता के रूप में तो आप मुझे जानते ही हैं, अत: चौंकने अथवा शंकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ न मैं किसी प्रकार का दौत्य करनेवाला हूँ और न किसी बात का समर्थन ही। –तो फिर मुझे कहना क्या है? और क्यों और कैसे?
युग-युगों से आप मेरी ‘गीता’ सुनते आ रहे हैं। बरसों से आप उद्धवगीता का भी अध्ययन करते आये हैं। मेरे जीवन की भी एक गीता है–श्रीकृष्णगीता, जिसे मैं किसी को नहीं–आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। वास्तव में इस गीता की ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है!
गीता में मैंने प्रिय सखा अर्जुन से कहा था कि “ऐसा समय न कभी था और न कभी होगा, जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था।” आज पुन: कहता हूँ कि वह बात मैंने केवल अर्जुन से ही नहीं कही थी। हर सजीव से, हर स्त्री-पुरुष से कही थी, और वह भी सदा के लिए। तत्त्व-रूप से, विचार-रूप से आज भी प्रत्येक चराचर में मैं विद्यमान हूँ।
सर्वप्रथम ‘समय’ का अभिप्राय जान लेना आवश्यक है। आज विज्ञान का युग है–केवल ज्ञान का नहीं–भौतिकी के ज्ञान विशेष का युग है। विज्ञान का कहना है कि समय अखण्ड है। उसका कोई आरम्भ अथवा अन्त नहीं है, वह अनन्त है। और यही बात मैं गीता में कब का कह चुका हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से–मैं ही काल हूँ–समय हूँ। क्या यह सच नहीं कि आपसे अपने मन की बातें करने का अधिकार मुझे कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा! चकरा गये? थोड़ा सोचिए, आपको यह अवश्य स्वीकार होगा।
अखण्ड और अनन्त समय के साथ-साथ जड़ और चैतन्यमय जीवन में भी निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशीलता ही इसका स्थायी भाव है। मानव सहित सम्पूर्ण जीव-सृष्टि कभी आचार-विचार के उच्चतम शिखर पर विराजमान होती है, तो कभी वह रसातल तक जा पहुँचती है। यही परिवर्तनशीलता है। चैतन्यमय जीवन अनन्त है, असीम है, चिरन्तन है। वृद्धि और विकास ही इसके लक्षण हैं। तो क्या परिवर्तनशील जीवन के साथ-साथ उसे जान लेने की भाषा में भी अन्तर नहीं आएगा? गीता के दूसरे अध्याय में अनेक प्रकारों से, अनेक दृष्टान्तों से मैंने अपने अन्दर के श्रीकृष्ण को स्पष्ट किया है।
परन्तु आज किस रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ? बाल्यावस्था में ही अलग-अलग नाम और रूप धारण करनेवाले, असुर-राक्षसों का खेल-खेल में अन्त करनेवाले गोपालकृष्ण के रूप में? जलक्रीड़ा करनेवाली गोपियों के वस्त्र चुराने की अक्षम्य लगनेवाली शरारत करनेवाले कन्हैया के रूप में? पहले गोपालों के मुखिया और बाद में यादवों के प्रमुख योद्धा के रूप में? पिता के घर में दही, दूध, माखन की विपुलता होते हुए भी अपने साथियों के संग गोपालों के घरों में दधि-माखन की चोरी करनेवाले नटखट बालकृष्ण के रूप में? ‘अवतार’ उपाधि का मोहक वस्त्र ओढ़नेवाले ऐन्द्रजालिक कृष्ण के रूप में? सही समय पर द्रौपदी की लज्जा-रक्षा हेतु….
युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download Free in this Post from Google Drive Link and Telegram Link , No tags for this post. All PDF Books Download Free and Read Online, युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download PDF , युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download Summary & Review. You can also Download such more Books Free - Hindi Novels PDF Download FreeHindi PDF Books Download
Description of युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download
| Name | युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download |
| Author | No tags for this post. |
| Category | Novels |
| Language | Hindi |
| Download Link | Working |
युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download link is given below
We have given below the link of Google Drive to download in युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download Free, from where you can easily save PDF in your mobile and computer. You will not have to pay any charge to download it. This book is in good quality PDF so that you won't have any problems reading it. Hope you'll like our effort and you'll definitely share the युगन्धर / Yugandhar Hindi Book PDF Download with your family and friends. Also, do comment and tell how did you like this book?